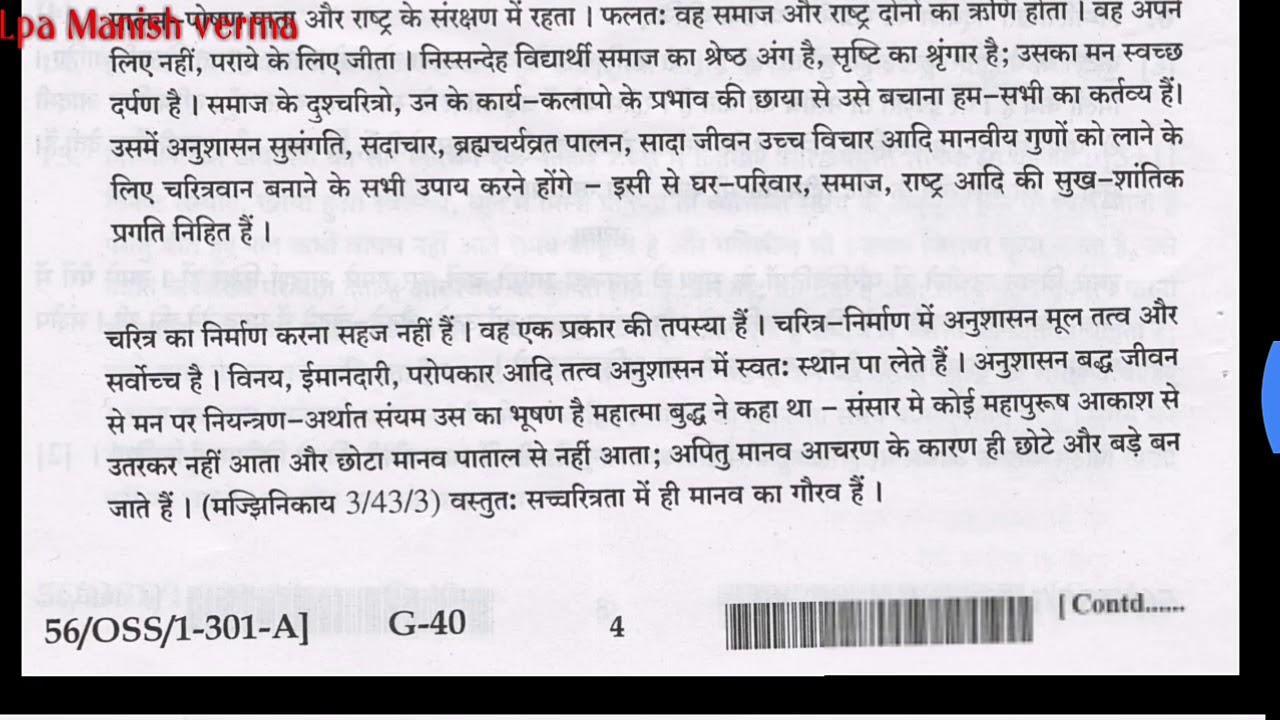
Hindi Book PDF Link:-
1. (क) निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए :
सखी म्हारी नींद नसाणी हो ।
पिय रो पंथ निहारत सब रैण बिहाणी हो ।
सखियन सब मिल सीख दयाँ मण एक णा मानी हो ।
बिन देख्याँ कल ना पड़ाँ मण रोस णा ठानी हो ।
अंग खीण व्याकुल भयाँ मुख पिय पिय बाणी हो ।
अंतर वेदन बिरह री म्हारी पीड़ णा जाणी हो ।
ज्यूँ चातक घणकूँ रटै, मछरी ज्यूँ पाणी हो । मीराँ व्याकुल बिरहणी, सुध बुध बिसराणी हो ॥
उत्तर –
प्रसंग – प्रस्तुत पद मीरांबाई पाठ से लिया गया है | पद में मीराँ ने विरह की वेदना को अभिव्यक्त किया है। विरहिणी की नींद उड़ जाना तथा प्रियतम के बिना किसी भाँति चैन न पड़ना – इस भाव को मीराँ ने अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।
व्याख्या – मीरा कहती हैं कि हे सखी, प्रियतम के वियोग में हमारी नींद जाती रही है, प्रियतम की राह देखते हुए सारी रात व्यतीत हो गई है। हालाँकि सारी सखियों ने मिलकर मुझे सीख दी थी, पर मेरे मन ने उनकी एक न मानी और मैंने कृष्ण से यह स्नेह संबंध जोड़ ही लिया। अब यह हालत है कि उन्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता और बैचेनी भी जैसे मुझे अच्छी लगने लगी है। मेरा सारा शरीर अत्यंत दुबला और व्याकुल हो गया है तथा मेरे मुख पर सिर्फ प्रियतम का ही नाम है। मीराँ कहती हैं, हे सखी! मेरे विरह ने मुझे जो आंतरिक पीड़ा दी है, उस पीड़ा को कोई नहीं जान पाता। जैसे चातक बादल की ओर एक टक दृष्टि लगाए रहता है और मछली पानी के बिना नहीं रह पाती, तड़पती रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं, अपने प्रियतम के लिए तड़पती हूँ। प्रिय के वियोग में मैं अत्यंत व्याकुल हो गई हूँ और इस व्याकुलता में मैं अपनी सुध-बुध भी खो बैठी हूँ।
विशेष –
- भाषा ब्रजभाषा है
- यह काव्य गतिकव्य है
- वियोग श्रृंगार रस है
Hindi Very Important Questions Answers
अथवा
स्पंदन में चिर निस्पंद बहा,
क्रंदन में आहत विश्व हँसा,
नयनों में दीपक से जलते,
पलकों में निर्झरिणी मचली !
मेरा पग-पग संगीतभरा,
श्वासों से स्वप्न पराग झरा,
नभ के नव रंग, बुनते दुकूल,
छाया में मलय बयार पली !
उत्तर-
प्रसंग – प्रस्तुत पद महादेवी वर्मा के पाठ से लिया गया है | कविता का अर्थ दो समानांतर स्तरों पर लगाया जा सकता है। पहला – जलपूर्ण उमड़ते-घुमड़ते बादल; और दूसरा-दुखी और वेदनाग्रस्त नारी, जो स्वयं कवयित्री भी हो सकती है।
व्याख्या- पहले ‘बदली’ के पक्ष में – बदलो की हर गर्जना के पीछे और हलचल के पीछे स्थिरता बसी है। मानो कोई है जिस पर इस क्रंदन(शोर) का कोई प्रभाव नहीं होता, वह निस्पंद रहता है। जबकि उस गर्जना पर विश्व प्रसन्न होता है क्योंकि वह भीषण गरमी से दुखी है, इसलिए बादलों की हलचल और गर्जन उन्हें प्रसन्न कर जाती है। बादलों में बसी विद्युत की कौंध दीपकों-सी प्रतीत होती है और उनमें स्थित जल नदी की भाँति प्रवाहित होने को आतुर है।
दूसरी ओर विरहिणी के पक्ष में – उसके स्पंदन में वह चिर निस्पंदन बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है, बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गर्जन | किसी की पीड़ा के स्वर नहीं, बल्कि कोई ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा हो परंतु यह किसी एक प्रेमी का क्रंदन है।विरहिणी की आँखों में दीपक से जलते रहते हैं। ये दीपक विरहाग्नि के भी हो सकते हैं और आशा के भी। आँसू उसकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर हैं वह अपनी विरह-वेदना को आँसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, कवयित्री कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं।
नीर भरी बदली अपनी स्थिति का आगे वर्णन कर रही है: मेरे तो कदम-कदम पर संगीत है- बिजली की कड़क, बादलों का गर्जन उसके आने की प्रसन्नता में मानव-जगत या पशु-जगत की हलचल ही मानो उसके पग-पग का संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी साँसें हैं, जिनसे पराग झरता है। उसे कवयित्री ने ‘स्वप्न-पराग’ कहा है। बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। नवरंगों से युक्त इंद्रधनुषी आभा ही मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र हैं। बादलों की छाया में मलय-बयार, शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। वही कवयित्री के शब्दों में ‘मलय-बयार’ है। वह कहती हैं कि प्रियतम की स्मृति मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल-मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है।
विशेष –
- खाड़ी बोली का प्र योग किया गया है
- विरह वेदना की अभिव्यक्ति है
- मानवीकरण अलंकर का प्रयोग है
- वियोग श्रृंगार रस है
Hindi Very Important Questions Answers
(ख) निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का काव्य-सौंदर्य स्पष्ट कीजिए :
सब घट अंतर रमसि निरंतर, मैं देखन नहिं जाना । गुन सब तोर, मोर सब औगुन, कृत उपकार न माना ॥
उत्तर –
भाव सौन्दर्य – यह पंक्तियां कवि रैदास के पद से ली गई है | यह कवि रैदास जी कहते है | है ! ईश्वर आप तो सभी जगह (घट) निवास करता है | मैं ही कभी आपको नही देख पाया | आपके अंदर गुण-ही-गुण है, जबकि मेरे अंदर अवगुण- ही अवगुण, आपने मुझ पर कितने उपकार किए हैं लेकिन मैं उनका महत्व नहीं समझ पाया।
शिल्प सौन्दर्य –
- कवि – रैदास
- पद ब्रजभाषा में रचित हैं |
- पद राग-रागनियों में बँधे हुए हैं
2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 35-35 शब्दों में लिखिए :
(क) रहीम ने ‘ओछे’ व्यक्ति की क्या विशेषता बताई है?
उत्तर – रहीम ने ‘ओछे’ व्यक्ति की तुलना एक शतरंज के प्यादे से कारी है | जब ओछे व्यक्ति को किसी कारणों से कोई पद या अधिक पैसे मिल जाते है तो वह इतराने लगते हैं तथा घमंडी हो जाते है | जैसे प्यादा वजीर के समान बनते ही उसकी तरह टेड़ा-टेड़ा चलने लगता है |
(ख) कवि राजेंद्र कठपुतली बने रहने को सुविधा क्यों कहते हैं?
उत्तर – कवि राजेन्द्र कठपुतली बने रहने को सुविधा इसलिए कहते है, क्यूँकि मनुष्यउन्हें प्राप्त खुशियाँ और जीवन जीने के बने-बनाए रास्ते तभी उपलब्ध हो सकते हैं, जब हम दूसरों का कहा करते रहें, अपनी डोर दूसरों के हाथों में दे दें। हम ऐसा कभी भय के कारण किया करते है, कभी भौतिक सुखों के लालच में कभी नौकरी बचाने के लिए किया करते है, कभी केवल इसलिए कि हमें बड़ों के आदेश का पालन करना है। कुल मिलाकर ऐसा करने के पीछे हमारा विवेक नहीं कोई भय, लोभ या जीवन की रूढ़ियाँ ही होती हैं।
(ग) भरत को माँ के प्रति आक्रोश क्यों था?
उत्तर – भरत को माँ के प्रति आक्रोश इसलिए था क्योंकि कैकयी ने राम और भारत के बीच अंतर डाल दिया था अर्थात राम को वनवास भेजने का वरदान माँगा था जिस कारण भारत बहुत शर्मिंदा थे उनको अपनी माँ पर क्रोध आ रहा था |
3. ‘परशुराम के उपदेश’ अथवा ‘वह तोड़ती पत्थर’ कविता का केंद्रीय भाव 30-40 शब्दों: स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर – वह तोड़ती पत्थर ‘सूर्यकांत त्रिपाठी निराला’ द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी कविता है। इस कविता में कवि ‘निराला’ जी ने एक पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया है। कवि निराला जी कहते हैं कि मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी लगन एवं निष्ठा से करते हैं फिर भी उनके मालिक जो संपन्न वर्ग के होते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और उन्हें अनेक तरह से प्रताड़ना प्रताड़ित करते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसके उपरान्त भी यह निर्बल श्रमिक लोग स्वाभिमान से से जीना जानते हैं और स्वाभिमान से जीने की क्षमता रखते हैं। वे ये क्षमता भी रखते हैं कि अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दें।
कविता का भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत है। सड़क पर पत्थर तोड़ती एक मजदूर महिला का वर्णन कवि ने अत्यंत सरल शब्दों में किया है। वो तपती दोपहरी में बैठी हुई पत्थर तोड़ रही है। वो एक साधारण परिवार की महिला है लेकिन उसका आचरण एकदम सरल और शुद्ध है। इस कविता के माध्यम से कवि ने श्रमिक वर्ग और संपन्न वर्ग दो विरोधी वर्गों के चित्र खींचे हैं और यह बताया है एक तरफ कठिन परिस्थितियों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग है तो दूसरी तरफ सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोग।
कवि निराजी जी अपनी सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ रखते हैं और शोषण करने वाली पाषाण हृदय सामाजिक व्यवस्था को धिक्कारते हुये उसके खंड-खंड होने की कामना करते हैं।
4. भारतेंदु युग अथवा द्विवेदी युग की दो काव्यगत विशेषताएँ बताइए ।
उत्तर –
- राष्ट्रीयता की भावना – भारतेंदु युग के कवियों ने देश-प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जन-मानस मे राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया।
- सामाजिक चेतना का विकास – भारतेंदु युग काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज मे व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएँ लिखीं।
- हास्य व्यंग्य – हास्य व्यंग्य शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किएगए।
- अंग्रेजी शिक्षा का विरोध – भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं मे प्रकट किया है।
5. निम्नलिखित काव्य-पंक्तियों में निहित रस और अलंकार का नाम बताइए:
कनक कनक तैं सौ गुनी, मादकता अधिकाय ।
वा खाएँ बौरात है, या पाएँ बौराय ॥
उत्तर – कनक (सोना) कनक (धतुरा या भंग) दोनों के अर्थ अलग-अकग हैं यहाँ यमक अलंकर का प्रयोग किया गया है |
6. निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए:
एक तेरी ही नहीं, सुनसान राहें और भी हैं
कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी हैं ।
और भी हैं ओंठ जिन पर
वेदना मुस्कान बनती
नींद तेरी ही न केवल
स्वप्न की पहचान बनती ।
पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं –
‘वाह’ बनने के लिए मजबूर आहें और भी हैं ।
एक नन्हा घोंसला
उड़ता न आँधी में अकेला,
पड़ गया पाला अगर
तो एक टहनी ने न झेला ।
सोच तो क्या बाढ़ आई है अकेले को डुबाने,
एक तिनका ढूँढती असहाय बाहें और भी हैं ।
तू अकेला ही नहीं है।
जो अकेला चल रहा है
और तलुवों के तले भी
यह धरातल जल रहा है
और हैं साथी जिन्हें तूने न देखा है न जाना
सामने है एक ही, लेकिन दिशाएँ और भी हैं ।
(क) कवि इन पंक्तियों में किसको सांत्वना देता जान पड़ता है?
उत्तर – कवि इन पंक्तियों में उन व्यक्तियों को सांत्वना ( तसल्ली ) देते हुए दिखाई देता है जो हताश और निराश बैठें हुएं हैं |
(ख) कवि उस व्यक्ति को क्या उदाहरण देकर सांत्वना देता है?
उत्तर – कवि उस व्यक्ति को अलग-अलग तरह के उदहारण देता है जैसे – तेज़ आंधी का, बाढ़ का कड़क ठंडी आदि का |
(ग) बाढ़ के समय क्या स्थिति होती है?
उत्तर – जब बाढ़ आती है तो वह सभी को डूबा देती है और लोग छोटे से भी सहरे के लिए अपनी बाहें फैलाये रखते हैं |
(घ) इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश दे रहा है?
उत्तर – इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते है की जो कठिन परिस्थितियां होती है वह सिर्फ एक मनुष्य के ही जीवन में नही आती वह सभी के जीवन में आती हैं | इसलिए हमे यह नही सोचना चाहिए की हम अकेले परेशानियों से घिरें हुए हैं |
(ड) आँधियों का घोंसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर – जब आँधियाँ चलती हैं तो तेज हवाएं घोंसलों को उड़ा कर कहीं दूर ले जाति हैं |
7. (क) निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए:
यह मन ही तो है, जिसमें चाह है, लक्ष्य है, वहीं उसमें पवित्रता, कोमलता व प्रियता है। उनका नवउत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य, सेवा कार्य में रमा रहता है । हर प्रकार की स्वच्छता की भावना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग रही है । बहुत से लोगों में यह स्वच्छता बाह्य रूप में ही मिलती है ।
उत्तर –
संदर्भ – यह यह गद्यांश प्रो. कैलाश चंद्र भाटिया द्वारा रचित ‘जिजीविषा की विजय’ नामक संस्मरण में से लिया गया है।
प्रसंग – यहं लेखक ने ‘मन’ को परिभाषित किया है मन की विशेषताओं को उजागर किया है, और डॉ रघुवंश के चरित्र में वह सारी विशेताएँ समाहित हैं |
व्याख्या – इस अनुच्छेद में लेखन ने ‘मन’ को कहा है की मन में चाह है, लक्ष्य है उसमे पवित्रता है, कोमलता है |इन्ही सारी विशेषताओं से डॉ. रघुवंश ने अपनी अपंगता को संवेगात्मक सशक्तता प्रदान की और मन में सुदृढ़ता से यह निश्चय किया कि यह अपंगता उनके जीवन के किसी कार्य में बाधक नहीं होगी और जीवन भर, उनके मन की सुदृढ़ता कायम रही और वे हर क्षेत्र में आगे बढ़े। यह स्वभाव उनके अंदर ही है उन्होंने दिखावा के लिए कभी नही अपनाया |
अथवा
दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं । सुखी वह है जिसका मन वश में हैं, दुखी वह है जिसका मन परवश है । परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दाँत निपोरना, चाटुकारिता, हाँ हजूरी । जिसका मन अपने वश में नहीं है, वही दूसरे के मन का छंदावर्त्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फँसाने के लिए जाल बिछाता है ।
उत्तर – दुख और सुख सच में मन के विकल्प हैं। लेखक के अनुसार जिस व्यक्ति का मन उसके वश में है, वह सुखी कहलाता है। कारण कोई उसे उसकी इच्छा के विना कष्ट नहीं दे सकता है। वह अपने मन अनुसार चलता है और जीवन जीता है। दुखी वह है, जो दूसरों के कहने पर चलता है या जिसका मन स्वयं के वश में न होकर अन्य के वश में है। वह उसकी इच्छानुसार व्यवहार करता है। उसे खुश करने के लिए ही सारे कार्य करता है। वह दूसरे के समान वनना चाहता है। अतः दूसरे के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अतः दुख और सुख तो मन के विकल्प ही हैं। जिसने मन को जीत लिया वह उस पर शासन करता है, नहीं तो दूसरे उस पर शासन करते हैं।
(ख) पठित पाठ के आधार पर रामचंद्र शुक्ल अथवा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा-शैली की दो विशेषताएँ लिखिए ।
उत्तर –
- रामचंद्र शुक्ल की भाषा-शैली की विशेषताएँ
- शुक्ल जी की भाषा में उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का यथा सम्भव प्रयोग हुआ है किन्तु ये अलंकार चमत्कार प्रदर्शन के लिये न होकर विषय को प्रभावशाली बनाने के लिये किये गये हैं।
- शुक्ल जी की भाषा परिष्कृत, प्रौढ़ एवं साहित्यिक है, जिसमें भाव प्रकाशन की अद्भुत क्षमता है।
- उनके निबन्धों की भाषा व्याकरण संवत होने के साथ-साथ अशुद्धियों से मुक्त है।
- विरामचिह्नों का प्रयोग अत्यन्त सहजता के साथ किया गया है।
- उनके भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें बोझिलपन एवं उलझन की स्थिति नहीं है।
- कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा-शैली की विशेषताएँ
उत्तर – प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतया तत्सम शब्द प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ीबोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग्य और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएँ हैं। वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटक-शैली के रूप इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं।
प्रभाकर जी के वाक्य-विन्यास में विविधता रहती है। चिन्तन की मनःस्थिति में भावुकता के क्षणों में इन्होंने व्याकरण के कठोर बन्धन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य-रचना भी की है। निश्चत ही ये हिन्दी के एक मौलिक शैलीकार हैं।
8. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर 35-35 शब्दों में दें:
(क) ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी की आबादी के बारे में क्या जानकारी दी?
उत्तर – ग्रेजुएट नवयुवक ने लेखक को कन्याकुमारी के शिक्षित युवकों की बेकारी के बारे में बताया। इन चार-पाँच सौ शिक्षित युवकों में लगभग सौ ग्रेजुएट थे। वे नौकरियों के लिए अर्जियाँ देते थे तथा आपस में दार्शनिक सिद्धान्तों पर बहस करते थे। वे कोई छोटा-मोटा काम करते थे। घाट के पास की चट्टान पर आत्महत्याएँ बहुत होती थीं।
(ख) शुक्ल जी के अनुसार क्रोध से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं?
उत्तर –
(ग) अरूणा और चित्रा के बीच अक्सर किन विषयों पर बहस हुआ करती थी?
उत्तर –
9.अनुराधा की किन्हीं दो चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ।
उत्तर – अनुराधा एक नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है यह अपने मां-बाप के लिए एक संस्कारवान बेटी है, तो छोटी बहन के लिए एक आदर्श, जो गांव की लाड़ली है होनहार बिटिया है, तो पति को दिलों जान से प्यार करने वाली नारी का एक रूप। परंतु कहीं न कहीं हमारे समाज में घूम फिरकर ऊंगली उठाने की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है।
एक नारी सब कुछ सह सकती है पर गलत नहीं सह सकती है। वह दुख सहती है पर जुंबा से आह नहीं करती है पर अनुराधा जैसे गुणवान लोगों को अगर यह समाज गलत समझने लगता है तो बाकी की बात ही क्या है।
10. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:
वाणी ईश्वर द्वारा दिया गया वह वरदान है जो प्राणियों को प्रकृति के अन्य उपादानों से श्रेष्ठ बनाती है । सुख-दुख के समय वाणी द्वारा की गई प्रतिक्रिया प्राणियों की भाव-स्थिति को प्रकट करती है । वाणी प्राणी की पहचान है । कौए और कोयल की पहचान उनकी वाणी से हो जाती है । रंग-रूप में समानता होने पर भी दोनों की वाणी ही उन्हें आदरित और अनादरित बनाती है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति के आचार-व्यवहार तथा स्वभाव की परख भी उसकी वाणी से ही होती है । मीठी वाणी दूसरों को वश में करने की औषधि है । जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं, तब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है । सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दुर्जनों की वाणी कटु तथा कर्कश होती है । मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है, निराश व्यक्तियों में आशा, उत्साह का संचार कर सकती है । कटु वाणी हृदय में शूल की तरह चुभती है । इससे अपने भी पराए हो जाते हैं । इतना ही नहीं, कटु वाणी लड़ाई-झगड़ों, यहाँ तक कि बड़े युद्ध का कारण भी बन जाती है । ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया । मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है ।
(क) प्रकृति के विभिन्न उपादानों में कौन श्रेष्ठ है और क्यों ?
उत्तर – प्रकृति के विभिन्न उपादानों में वाणी श्रेष्ठ है क्योंकि वाणी प्राणी की पहचान है | सुख-दुख के समय वाणी द्वारा की गई प्रतिक्रिया प्राणियों की भाव-स्थिति को प्रकट करती है |
(ख) सज्जनों और दुर्जनों की वाणी में क्या अंतर है ? उदाहरण सहित बताइए ।
उत्तर – सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दुर्जनों की वाणी कटु तथा कर्कश होती है ।
(ग) हमारा चित्त कैसी वाणी के श्रवण से प्रसन्न हो जाता है ?
उत्तर – जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं, तब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है । सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि दुर्जनों की वाणी कटु तथा कर्कश होती है । मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है, निराश व्यक्तियों में आशा, उत्साह का संचार कर सकती है । कटु वाणी हृदय में शूल की तरह चुभती है ।
(घ) मनुष्य सब कुछ कैसे पा सकता है?
उत्तर – जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया ।
(ड) गद्यांश के अनुसार अमृत के समान कौन काम कर सकता है ?
उत्तर – मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है ।
(च) गद्यांश में से ‘मधुर’ और ‘निराशा’ शब्दों के विलोम शब्द छाँटकर लिखिए ।
उत्तर –
- मधुर – कटु, कर्कश
- निराशा – आशा
(छ) ‘आदरित’ शब्द में से मूल शब्द एवं प्रत्यय छाँटकर अलग-अलग लिखिए ।
उत्तर – आदर +इत
(ज) ‘दुर्जन’ एवं ‘सज्जन’ शब्दों में लगे उपसर्ग छाँटिए ।
उत्तर – दूर+जन, सत + जन
(झ) गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए ।
उत्तर – वाणी अमृत के समान
11 निम्नलिखित वाक्य में उचित स्थान पर विराम-चिह्न लगाइए :
(क) देश वीरांगनाओं का मान सम्मान करेगा
उत्तर – देश वीरांगनाओं का मान सम्मान करेगा |
(ख) निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए :
चाय का एक गर्म प्याला पीते जाइए ।
उत्तर – चाय का एक गरम प्याला पीते जाइए ।
(ग) निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए :
परीक्षाएँ समाप्त होने के बाद सभी बच्चे खेलने में लग गए । (मिश्र वाक्य में बदलिए)
उत्तर- परीक्षाएँ समाप्त हुई और सभी बच्चे खेलने में लग गए |
(घ) अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए:
विजय आज परीक्षा देने के बाद खेलने नहीं आएगा ।
उत्तर – संकेतवाचक वाक्य
(ड) निर्देशानुसार वाच्य-परिवर्तन कीजिए :
हम नहीं दौड़ते । (भाववाच्य में बदलिए)
उत्तर – हम से दौड़ा नही जाता
12. (क) कुंजर सिंह अथवा कुमुद के चरित्र की तीन विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर –
- कुंजर सिंह की तीन विशेषताएँ
- कुंजर सिंह दासी पुत्र होने के कारण राज सिंहासन का अधिकारी नहीं है।
- देशभक्त है। देवीसिंह के राज्यासीन होने पर विद्रोह कर देता है।
- वह स्वाभिमानी प्रकृति का है और राष्ट्र की आन बचाने के लिए विदेशी सहायता लेने से इंकार कर देता है और देश व प्रेम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है।
- कुमुद के चरित्र की तीन विशेषताएँ
- कुमुद जन्म से अत्यंत सुन्दर है। किशोरावस्था में पहुंचते-पहुंचते उसकी ख्याति चारो तरफ फेल जाती है। लोग उसे दुर्गा का अवतार मानते थे।
- कुमुद का प्रेमी हृदय है। वह कुमार सिंह से प्रेम करती है।
- कुमुद को जब अलीमर्दान अपने नापाक हाथो से स्पर्श करना चाहता है तो वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेतवा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राणो का विसर्जन कर देती है।
(ख) स्पष्ट कीजिए कि ‘विराटा की पदमिनी’ उपन्यास का कथानक सामंती परिवेश को उद्घाटित करता है ।
उत्तर –
i. विराटा की पद्मिनी के संवाद सरस हैं और रोचक है।
ii. संवाद पात्रानुकूल हैं और उनमे परिस्थिति की मांग झलकती है।
iii. दरबारियों के संवादों में चाटुकारिता, छल-कपट और मरने-मारने की शब्दावली है।
13. (क) बड़ी रानी ने छोटी रानी के विद्रोह में शामिल होने का निश्चय क्यों किया ?
उत्तर – छोटी रानी ने बड़ी रानी को अपनी मीठी, चिकनी-चुपड़ी बातो से अपनी तरफ कर लिया। उसने बड़ी रानी को यह भी यकीन दिलाया कि उनके महल से बहार निकलते ही देवी सिंह से असंतुष्ट सरदार उनकी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे।
(ख) सबदल सिंह कुंजर सिंह को आश्रय देने से क्यों हिचकता है ?
14 निम्नलिखित में से किसी एक का भाव-पल्लवन कीजिए :
(क) जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन
उत्तर – संगति का प्रभाव मनुष्य पर जरुर पड़ता है I जिस प्रकार स्वाति कि बूँद सीप के सम्पर्क में आने पर मोती, और सर्प के सम्पर्क में आने पर विष बन जाती है उसी प्रकार सत्संगति में रहकर मनुष्य का आत्मसंस्कार होता है जबकि बुरी संगति उसके पतन का कारण बनती है I अच्छी संगति में रहकर मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है, उसकी बुद्धि परिष्कृत होती है और उसका मन शुद्ध होता है I बुरी संगति हमारे भीतर के दानव को जागृत करती है I
(ख) अपना भाग्य, अपने हाथ
उत्तर –
15 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए :
(क) युवा वर्ग में बढ़ती नशे की लत
(ख) प्रदूषण – एक महादानव
(ग) अनुशासन और हम
(घ) भारत की प्राकृतिक सुंदरता
उत्तर – हमारा देश भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल और विस्तृत है बल्कि वह अपनी विभिन्न प्राकृतिक सुन्दरता के कारण भी बहुत बड़ा देश है । भारत की प्राकृतिक सुन्दरता सचमुच में निराली और अद्भुत है ।
अपनी इस अद्भुत सुन्दरता के कारण ही भारत विश्व का एक अनोखा और महान् राष्ट्र समझा जाता है । अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के साथ-साथ भारत की भौतिक सुन्दरता भी कम आकर्षक और रोचक नहीं है । हमारा देश अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण सबके आकर्षण का केन्द्र रहा है । यह उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ।
पूरब में मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ अपने सौन्दर्य और छवि से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । हमारे देश की छवि चारों ओर से अधिक-से-अधिक मनमोहक रूप में दिखाई पड़ती है । इसके उत्तर में विश्व का सबसे ऊँची श्रेणियों वाला पर्वत हिमालय स्थित है । इसकी बर्फ की चोटियों को देखकर ऐसा लगता है कि मेरे देश ने सफेद पगड़ी या मुकुट धारण कर लिया है ।
यहाँ बहने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु जैसी नदियाँ इस देश के गले में पड़ी हुई मोतियों की माला के समान शोभा को बढ़ाने वाली हैं । दक्षिण में हिन्द महासागर की कल्लोल करती हुई ऊँची-ऊँची तरंगे इस देश का चरण स्पर्श करके इसके चरणों को पखारती हुई मधुर-मधुर गान किया करती है ।
हमारे भारत देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी विविध प्रकार की है । यहाँ हर प्रकार की जातियाँ, धर्म, रिवाज, पर्व, त्योहार, दर्शन, साहित्य, आचरण आदि सब कुछ एक दूसरे से न मिलते हुए भी एक ही दिखाई देते हैं । हमारे देश के पूर्व-त्योहार जो समय-समय पर सम्पन्न होते रहते हैं । वे वास्तव में दर्शनीय और आकर्षक हैं ।
हमारे उत्तरी क्षेत्र में दर्शनीय स्थानों की अधिकता और विशालता है । इस क्षेत्र के जो भी दर्शनीय स्थल हैं वे अपनी कला और संस्कृति के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण हैं-संसार का आठवां आश्चर्य आगरे का ताजमहल, सिकन्दराबाद, फतहपुर सीकरी, मथुरा, वृन्दावन, डींग, भरतपुर आदि विश्व के प्राय: सभी व्यक्तियों के आकर्षण के एकमात्र केन्द्र हैं ।
भगवान विश्वम्भर कैलाशपति भूतभावन शंकर की नगरी काशी का न केवल ऐतिहासिक महत्त्व है और न केवल धार्मिक ही है अपितु पौराणिक और सांस्कृतिक महत्त्व भी कम नहीं है । इसके पास ही में स्थित इलाहाबाद (प्रयाग) की त्रिवेणी का महत्त्व न केवल वैदिक और पौराणिक काल से ही है, इसके पास महान् हिन्दू सम्राट अशोक का किला का महत्त्व आज भी ज्यों-का-त्यों है ।
राणा प्रताप और राणा सांगा की जन्मभूमि पद्मिनी की सुन्दरता, बलिदान और त्याग की भूमि राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, माउण्टआबू और जयपुर एक अनोखा और सुन्दरता का महान् केन्द्र है । इसी तरह से कुल्लू, मनाली, कांगड़ा की दर्शनीय छटा और कश्मीर की कुम्कुम और केशर की क्यारियाँ हमारे आकर्षण के अलग-अलग केन्द्र हैं ।
कश्मीर की विभिन्न फूलों की घाटियाँ, फल-पत्तों से ढके हुए हिम-शिखरों पर पड़ती हुई सूर्य-चन्द्रमा की किरणें हमें अपनी ओर बार-बार मोह लेती हैं । हमारे देश की शोभा कितनी अद्भुत है, इसे कौन नहीं जानता है । झेलम के तट पर स्थित श्रीनगर, चमकीली, डल झील की शोभा, शालीमार, निशात बाग, गुलमर्ग का मैदान, पहलगाम की खूबसूरती, अमरनाथ प्रसिद्ध तीर्थ हैं ।
इसी तरह से देश के उत्तरी भाग की प्राकृतिक शोभा में मानसरोवर अल्मोड़ा, कोसानी, नैनीताल, मंसूरी, चंडीगढ़, अमृतसर आदि प्रसिद्ध हैं । हमारे देश का पश्चिमी भाग की पर्यटकों सहित अनेक दर्शकों के मनों को एक साथ ही अपने आकर्षण में बाँध लेता है । अजन्ता, एलोरा की गुफाएँ बम्बई के ऊँची-ऊँची समुद्र, तटीय अट्टालिकाएँ, शिवाजी का कर्म क्षेत्र, पूना का वह पवित्र स्थल, गोवा आदि प्रकृति के अद्भुत आकर्षण हैं ।
अहमदाबाद कला-कृति का अद्भुत स्थल इसी पश्चिमी क्षेत्र में है । द्वारिकापुरी का पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व, साँची के स्तूप, विदिशा, खजुराहो, उज्जैन पचमढ़ी, ग्वालियर, जबलपुर ऐसे नगर परिक्षेत्र हैं, जो न केवल अपनी संस्कृति, कलाकृतियों और रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अपितु अपने इतिहास और कार्य-व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं ।
उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र की तरह भारत का पूर्वी भाग भी कम आकर्षण का केन्द्र नहीं है । आसाम, बंगाल, बिहार आदि राज्य इस पूर्वी भाग के अन्तर्गत आते हैं । आसाम के चाय के बाग और मैदान, घाटियाँ, मणिपुर के विशाल आकर्षक प्राकृतिक छटा, बिहार और उड़ीसा के विस्तृत कृषि-क्षेत्र आदि पर्यटन के विशेष केन्द्र हैं ।
भगवान बुद्ध और महावीर, राम-कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जगन्नाथपुरी का मन्दिर, कोणार्क का मन्दिर, पटना का इतिहास, गया का गया माहाल्य आदि प्राचीन काल से ही अपनी महानता का परिचय दे रहे हैं । हमारे देश भारत का दक्षिणांचल भी अनेक दर्शनीय स्थल से पूर्णरूप से सम्पन्न है ।
आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, मैसूर राज्य, केरल राज्य आदि की प्राकृतिक शोभा कम सुन्दर और दर्शनीय नहीं हैं । इसके अन्तर्गत हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, महाबलीपुरम्, मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, बंगलौर, तंजौर की प्राकृतिक छटा, ऐतिहासिक महत्त्व, सांस्कृतिक प्रभाव और धार्मिक मान्यता हमारे जीवन को बार-बार जागरण संदेश देते हैं ।
केरल जो आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है, अवश्य दर्शनीय है । इसकी प्राकृतिक शोभा भी हमें बार-बार आकर्षित करती है । दक्षिण का समुद्र-तटीय मैदान भी कम दर्शनीय नहीं है । इस तरह हमारा देश भारत विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थलों का महाकेन्द्र होने के कारण विश्व का सचमुच में एक अनूठा राष्ट्र है ।
- कविता कैसें पढ़े || Nios Class 12th Hindi Chapter 1st.
- Nios Class 12th Hindi { यही आता है Exam में }
- NIOS Class 12th – Hindi Very Important Questions With Answers
- Nios Class 12th Hindi – प्रतिवेदन तथा प्रारूपण
- 9, Nios Class 12th Hindi – कोष्ठक कैसें करें ?
- Nios Class 12th Hindi – पत्र कैसें लिखें
- 2#, Nios Class 12th Hindi – काव्य सौंदर्य कैसें करें
- 1#, Nios Class 12th Hindi – सप्रसंग व्याख्या कैसें करें
- 2#, Nios Class 12th Hindi – काव्य सौंदर्य कैसें करें
- 3#, Nios Class 12th Hindi Very Important Questions With Answers
- 4#, Nios Class 12th Hindi – भाव पल्लवन किसे कहते हैं ?
- NIOS CLASS 12th Hindi Most Important Questions With Answers & Grammar Solutions
- Nios Class 12th Hindi || Blueprint
- Nios Class 12th Hindi Marathon || Full Syllabus
- Nios Class 12th Hindi – टिप्पणी और टिप्पण
16. अपने किसी प्रिय कार्यक्रम के प्रसारण के लिए धन्यवाद देते हुए और उसके पुनःप्रसारण की प्रार्थना करते हुए दूरदर्शन निदेशक को पत्र लिखिए ।
उत्तर –
17 दिल्ली में सफाई व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रतिवेदन तैयार कीजिए जिसमें इसके कारण होने वाली कठिनाइयों एवं भविष्य की चिंताओं का उल्लेख हो ।
उत्तर –
अथवा
निम्नलिखित गद्यांश का सार एक-तिहाई शब्दों में लिखिए एवं उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए :
बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया जाए यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जा सकता परंतु इसके कारण समाज में अपराध, हिंसा, लूटपाट, डकैती, चोरी, अपहरण व अन्य आर्थिक अपराध पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं । मनुष्य को अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं पर अंकुश लगा पाना असंभव सा है और इन्हें पूरा करने के लिए वह अनैतिक होकर अपराध के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है । सरकार को चाहिए कि वह एक रणनीति तैयार करे । विकास और रोजगार की ओर अग्रसर होते मार्ग को नई दिशा दी जाए । ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर व लघु उद्योगों को न सिर्फ प्रोत्साहन दिया जाए अपितु उन्हें आर्थिक सहायता देकर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है । सुदृढ़ एवं संगठित शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा को वैकल्पिक तौर पर नहीं, अनिवार्यता के आधार पर लागू करना चाहिए । नागरिकों को स्वावलंबन के लिए मशीनीकरण का ज्ञान भी उपलब्ध करवाना चाहिए । बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए परिवार नियोजन को अपनाकर जनसंख्या पर रोक लगाना भी आवश्यक है। ये जनता एवं सरकार दोनों को मिलकर करना होगा ।
18 किसी दुर्घटना में अपने बाल-बाल बचने के अनुभव को लगभग 40 शब्दों में व्यक्त कीजिए ।
उत्तर –
19. विद्यालय में कक्षा दसवीं के बाद विभिन्न विषयों के चयन के लिए 150 विद्यार्थियों ने जिन विशिष्ट विषयों को चुना उसका विवरण दिया जा रहा है । विवरण को दंड चित्र (बार ग्राफ) के रूप में प्रस्तुत कीजिए :
जीव विज्ञान
गणित
राजनीति विज्ञान
इतिहास
अर्थशास्त्र
गृह विज्ञान
टंकण कंप्यूटर
20. टिप्पण किसे कहते हैं ? कार्यालयी टिप्पण के दो उदाहरण दीजिए ।
उत्तर – टिप्पणी का अर्थ है- पत्र अथवा पत्र-संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी तथा टिप्पणीकार का कार्यालय के विधिविधान के अन्तर्गत उस पर अपना सुझाव देना। दूसरा- वांछनीय विषय अथवा पत्र-व्यवहार पर अपने विचारों को स्पष्ट करना। तीसरा- यह स्पष्ट करना कि ‘आवती’ के अंतिम निर्वाण के लिए क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।
Ø टिप्पण के प्रकारः
- सूक्ष्म टिप्पण
- सामान्य टिप्पण
- संपूर्ण टिप्पण
खण्ड – ‘ख’ (सूचना प्रौद्योगिकी और हिन्दी)
21 निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखिए :
(क) स्वच्छ प्रति
(ख) प्रायोजित कार्यक्रम
(ग) संवाददाता सम्मेलन का
22 (क) समाचार संपादक का क्या कार्य होता है ?
उत्तर – समाचार-पत्र के संपादकीय कार्य का निर्देशन एवं निरीक्षण का महत् दायित्व संपादक के कंधों पर होता है। संपादकीय नीति की दूरी होता है संपादक।
(ख) समाचार प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं ?
उत्तर – समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं –
- सरकारी स्रोत
- पुलिस विभाग एवं अदालत
- व्यक्तिगत स्रोत
- अस्पताल
- भेंटवार्ता
23 (क) ‘कार्टून वास्तव में स्वस्थ लोकतंत्र का लक्षण है ।’ – कैसे ?
उत्तर –
(ख) हिन्दी अखबारों की भाषा में एकरूपता का अभाव होने का क्या कारण है ?
उत्तर – हिंदी अखबारों की भाषा में एकरूपता का अभाव होने का कारण यह भी है कि हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी के विषय में अभी तक एकरूपता कायम नहीं की जा सकी है। इसका कारण यह है कि संस्कृत व्याकरण से हिंदी के शब्दों की वर्तनी को नियमित करना संस्कृत न जानने वाले हिंदी प्रेमियों को स्वीकार्य नहीं है।
24 (क) आपकी कंपनी ने झड़ते बालों के उपचार के लिए जड़ी-बूटियों से एक विशेष प्रकार का तेल तैयार किया है । उसकी विशेषताओं के प्रचार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, जिसे मुद्रण माध्यम से प्रकाशित किया जा सके ।
उत्त्तर –
(ख) बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के कारण चिंतित सरकार ने वाहनों में प्रेशर हॉर्न बजाने और शादी ब्याह में जोर से लाउड-स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है । इसी के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाचार-आइटम तैयार कीजिए ।
उत्तर –
खण्ड – ‘ग’ (विज्ञान की भाषा हिन्दी)
21 निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ स्पष्ट कीजिए :
(क) ई-कामर्स – ई-कॉमर्स, या बस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक संचार या नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन सामानों को वितरित करने, खरीदने, बेचने, या बाजार की वस्तुओं और सेवाओं, और धन के हस्तांतरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है।
(ख) पेजिंग
(ग) जीवाश्म – पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाये जाते हैं उन्हें जीवाश्म (जीव + अश्म = पत्थर) कहते हैं।
22. पर्यावरण प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि से किस प्रकार जुड़ा है ?
उत्तर –
अथवा
उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि किसी अंधविश्वास को तर्क के सहारे कैसे दूर किया जा सकता है ?
उत्तर –
23 (क) भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त का क्या योगदान रहा है ?
उत्तर – 598-668 ई के दौरान जाने-माने खगोलविदों में से एक रहे ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट के सिद्धांत को पुष्ट करके योगदान दिया कि मध्यरात्रि में एक नया दिन शुरू होता है। साथ ही उन्होंने यह दावा करते हुए आगे योगदान दिया कि ग्रहों की अपनी गति है जबकि उन्होंने लंबन के लिए सही समीकरण दिया और ग्रहण की गणना के बारे में जानकारी दी। ब्रह्मगुप्त का जन्म 598 ई में हुआ था। वह चावड़ा वंश के शासक व्याघ्रमुख के शासनकाल के दौरान राजस्थान में रहते थे। वह जिष्णुगुप्त के पुत्र थे और शैव हिन्दू ब्राह्मण थे। प्रथुदका स्वमीन, बाद के टिप्पणीकार ने उन्हें भिलामालाचार्य कहा, जो भिलामाला के शिक्षक थे।
न्होंने भारतीय खगोल विज्ञान पर पांच पारंपरिक सिद्धार्थ और साथ ही आर्यभट्ट I, लतादेव, प्रद्युम्न, वराहमिहिर, सिम्हा, श्रीसेना, विजयनंदिन और विष्णुचंद्र सहित अन्य खगोलविदों के काम का अध्ययन किया। वर्ष 628 में, 30 वर्ष की आयु में, उन्होंने ‘ब्रह्मस्सुफसिद्धांत’ (ब्रह्मा का सुधारा हुआ ग्रंथ) की रचना की, जिसे ब्रह्मपक्ष विद्यालय के प्राप्त सिद्धान्त का संशोधित संस्करण माना जाता है। विद्वानों ने कहा कि उन्होंने अपने संशोधन में मौलिकता का एक बड़ा हिस्सा शामिल किया, जिसमें काफी नई सामग्री शामिल थी।
67 वर्ष की आयु में, उन्होंने अपने अगले प्रसिद्ध काम खंड-खदिका की रचना की, जो कि कैराना श्रेणी में भारतीय खगोल विज्ञान के एक व्यावहारिक मैनुअल का उपयोग छात्रों द्वारा किया जाता था।ब्रह्मगुप्त के कार्य को ब्रह्मस्फुटा के रूप में जाना जाता है जो 14 सिद्धान्त का एक स्वैच्छिक कार्य है। मुख्य विषय जो किताब के पहले संस्करणों में शामिल हैं। इसमें ग्रहों की गति, सच्चे ग्रहों की गति, समय, स्थान और दूरी की समस्याएं, चंद्र और सौर ग्रहण, ग्रहों की वृद्धि और सेटिंग्स, चंद्रमा के ग्रह और छाया शामिल हैं।
उन्होंने पृथ्वी के घूर्णी गति को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की छाया के कारण ग्रहण पर विश्वास करने और राहु और केतु के पारंपरिक सिद्धांत के साथ खुद को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए आर्यभट्ट की आलोचना की। उन्होंने ग्रहों की नियमित गति, देशांतर और अक्षांश में लंबन के सही समीकरण, सही समीकरण और वालना की बेहतर अभिव्यक्ति की गणना के लिए तात्कालिक विधि खोजने के तरीके दिए। कहा जाता है उनका स्वर्गवास उज्जैन में ही हुआ।
(ख) भू-विज्ञान दक्षता क्यों अनिवार्य है ?
24 (क) सामान्य भाषा और वैज्ञानिक भाषा के दो अंतर समझाइए ।
उत्तर – भाषा विज्ञान के अध्येता ‘भाषाविज्ञानी’ कहलाते हैं। भाषाविज्ञान, व्याकरण से भिन्न है। व्याकरण में किसी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन (functional description) किया जाता है जबकि भाषाविज्ञानी इसके आगे जाकर भाषा का अत्यन्त व्यापक अध्ययन करता है।
(ख) बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है ? समझाइए ।
उत्तर – बढ़ती जनसंख्या की विकरालता का सीधा प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है जो जनसंख्या के आधिक्य से अपना संतुलन बैठाती है और फिर प्रारम्भ होता है असंतुलित प्रकृति का क्रूरतम तांडव जिससे हमारा समस्त जैव मण्डल प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस बात की चेतावनी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व माल्थस नामक अर्थशास्त्री ने अपने एक लेख में दी थी। इस लेख में माल्थस ने लिखा है कि यदि आत्मसंयम और कृत्रिम साधनों से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।
यदि आज हम अपने चारों ओर के वातावरण के संदर्भ में विचार करें तो पाएँगे कि प्रकृति ने अपना क्रोध प्रकट करना प्रारम्भ कर दिया है। आज सबसे बड़ा संकट ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रभाव से वातावरण के प्रदूषण के साथ पृथ्वी का ताप बढ़ने और समुद्र जल स्तर के ऊपर उठने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव वायुमण्डल में कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न होता है। ये गैस पृथ्वी द्वारा अवशोषित सूर्य ऊष्मा के पुनः विकरण के समय ऊष्मा का बहुत बड़ा भाग स्वयं शोषित करके पुनः भूसतह को वापस कर देती है जिससे पृथ्वी के निचले वायुमण्डल में अतिरिक्त ऊष्मा के जमाव के कारण पृथ्वी का तापक्रम बढ़ जाता है। तापक्रम के लगातार बढ़ते जाने के कारण आर्कटिक समुद्र और अंटार्कटिका महाद्वीप के विशाल हिमखण्डों के पिघलने के कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है जिससे समुद्र तटों से घिरे कई राष्ट्रों के अस्तित्व को संकट उत्पन्न हो गया है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आज से पचास वर्ष के बाद मालद्वीप देश समुद्र में डूब जाएगा। भारत के समुद्रतटीय क्षेत्रों के सम्बंध में भी ऐसी ही आशंका व्यक्त की जा रही है।
वायुमण्डल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या की निरंतर बढ़ रही आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। जब एक देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की संख्या बढ़ जाती है। आवास समस्या के निराकरण के रूप में शहरों का फैलाव बढ़ जाता है जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई होती है। दूर-दूर बस रहे शहरों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के बहाने वाहनों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ जाता है जिससे वायु प्रदूषण की समस्या भी उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इस तरह बढ़ती जनसंख्या हमारे पर्यावरण को तीन प्रमुख प्रकारों से प्रभावित करती है।
आज आवश्यकता है कि बढ़ती जनसंख्या पर कारगर रोक लगायी जाए ताकि वर्तमान एवं भविष्य में आने वाली मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल सके।